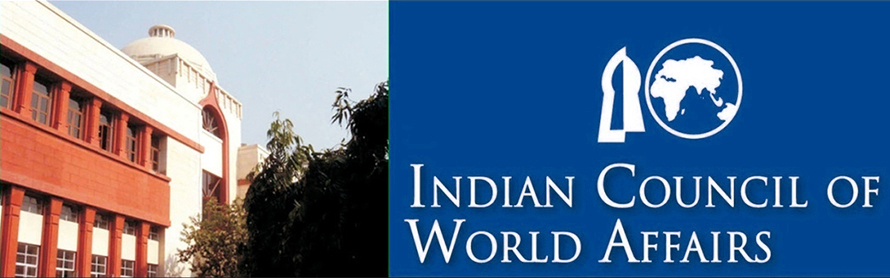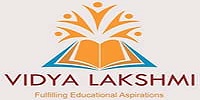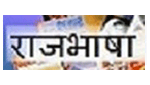भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली'हिंद महासागर में भारत और द्वीप राज्य: विकसित भू-राजनीति और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य' संगोष्ठी में श्री संजय बारू, सदस्य, शासी निकाय, आईसीडब्ल्यूए द्वारा मुख्य भाषण, 6 सितंबर 2022।
यह संगोष्ठी एक दिलचस्प समय पर आयोजित की जा रही है जब भारत ने अभी– अभी एक नया विमान कैरियर का शुभारंभ किया है और चीनी नौसेना का एक जहाज श्रीलंका के तट पर है। यूरोपीय शक्तियां, विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, हिन्द महासागर में नए सिरे से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, यह जल निकाय जो अब तक 'शांति क्षेत्र' बना हुआ था, ने विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरु कर दिया है। इसलिए, इस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आने वाले देशों के लिए यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में हमारे पास संघर्ष की एकमात्र स्मृति उन शक्तियों से जुड़ी है जो बाहर से इन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। हमारा आपस में कभी टकराव नहीं हुआ है।
सुमद्री इतिहासकार के. एम. पन्निकर ने अपने उत्कृष्ट निबंध, इंडिया एंड द इंडियन ओशन: एन एसे ऑन द इंफ्लूएंस ऑफ सी पावर ऑन इंडिनय हिस्ट्री (1945) में उल्लेख किया है, “कोलंबस के अटलांटिक और मैगलन के प्रशांत महासागर को पार करने से हजारों वर्ष पहले हिन्द महासागर वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का सक्रिए मार्ग बन चुका था।” [1] फिर भी, काफी समय तक अकादमिक साहित्य और नीति विश्लेषण का अधिकांश ध्यान समुद्री सुरक्षा, समुद्री शक्ति और नौसेना की रणनीति पर रहा, जिसमें संपूर्ण समुद्री आर्थिक विकास, सुमद्री संरचनात्मक ढांचे में निवेश, समुद्री संपर्क और वाणिज्य पर बहुत कम ध्यान दिया गया।
इसलिए, ब्लू इकॉनमी के विकास और समुद्र क्षेत्र के बारे में जागरुकता पर भारत का हालिया फोकस, भले ही यह क्षेत्र बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से ग्रसित हो, हिन्द महासागर में विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से शुभ संकेत है। [2]
पन्निकर ने निश्चित रूप से समुद्र के सामरिक महत्व पर ज़ोर दिया था और उनका मानना था कि हिन्द महासागर का “नियंत्रण” और मलक्का जलडमरूमध्य, अदन की खाड़ी और दक्षिणी विस्तार समेत इसके भीतर और बाहर के सभी 'चोक प्वाइंट्स' पर बाहरी आक्रमण से भारत की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मॉरीशस के पास समुद्र का हिस्सा भारतीय हाथों में होना चाहिए। [3] 15वीं से 18 वीं सदी तक सभ्यता और पूंजीवाद के अपने उत्कृष्ट अध्ययन में, इतिहासकार फर्नांड ब्राउडल ने हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की प्रमुख उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया था।[4] अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर– जिसे अब हिन्द– प्रशांत कहा जाता है, में फैले क्षेत्र का उल्लेख करते हुए इसे पूर्व–औद्योगिक, पूर्व– पूंजीवादी युग् के "विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी" के रूप में बताया जाता है। [5]
“इन विशाल क्षेत्रों के बीच संबंध,” ब्रूडेल ने लिखा, “अधिक या कम शक्ति वाले लोलक आंदोलनों की एक श्रृंखला का परिणाम था जो केंद्रीय रूप से स्थित भारतीय उपमहाद्वीप के दोनों ओर था। इसमें पहले पूर्व और फिर पश्चिम को– कार्यों, अधिकारों एवं राजनीतिक या आर्थिक उन्नति के पुनर्वितरण, का लाभ हो सकता है। इन सभी उलटफेरों के बावजूद, भारत ने अपनी केंद्रीय स्थिति बनाए रखीः गुजरात और मालाबार एवं कोरोमंडल के तट पर इसके व्यापारी सदियों तक अपने अनेकों प्रतिस्पर्धियों– लाल सागर के अरब व्यापारी, खाड़ी के फारसी व्यापारी या इंडोनेशियाई समुद्रों के जानकार चीन के व्यापारी, जिनके लिए अब वो आम रास्ता जैसा हो चुका था, के खिलाफ जीतते रहे।”[6]
यूरोपियों के इस क्षेत्र में आने से पूर्व हिन्द महासागर का भू–अर्थशास्त्र ऐसा ही था। जैसा कि इतिहासकार संजय सुब्रह्मण्यम कहते हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के बंदरगाहों के भारत के समुद्र संबंध बनने से बहुत पहले, भारत के “अपना जहाज रखने वाले व्यापारी” सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली और कालीकट जैसे बंदरगाहों से विश्व के साथ व्यापार किया करते थे।[7] आशिन दास गुप्ता 'हिन्द महासागर के व्यापारियों का विश्व' पर अपने विशाल शोध को इस प्रकार सारांशित किया:
“इसमें कोई शक नहीं कि 17वी सदी के बाद के समृद्ध वर्षों में ऐसे कुछ एक हजार लोग प्रत्येक वर्ष यात्रा पर निकलते और भारत के विदेश व्यापार को बढ़ावा देते एवं हिन्द महासागर की दुनिया के साथ भारत के संबंध गहरे बनाते …. ये ऐसे लोग थे जो बंदरगाह पर रहते हुए हर प्रकार से वाणिज्यिक जहाजों की सेवा किया करते थे। वे अपने जहाजों में माल लाए; उन्होंने आयात की बिक्री की व्यवस्था की; उन्होंने यात्रियों की यात्रा हेतु धन की व्यवस्था कर उनकी यात्रा को संभव बनाया। वे सामान्य वस्तुओं के व्यापारी थे; वे विशेष वस्तुओं के व्यापारी थे; वे पैसों के सौदागर थे और इन सब से बढ़कर वे बंदरगाह शहरों के दलाल थे। … लगभग 1630 के दशक में आरंभ हुई इस जादुई सदी में भारत के समुद्री व्यापारी, उचित रूप से कहा जाए तो इस सेवा क्षेत्र पर निर्भर थे और उन्हें सहायता भी प्राप्त हुई थी।” [8]
यूरोपीय व्यापारियों और नौसेनाओं के प्रवेश से दास गुप्ता ने जिसे भारतीय समुद्री गतिविधि का “जादुई सदी” कहा था, समाप्त हो गया। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने इसके आसपास के क्षेत्रों के साथ भारत के संबंधों की प्रकृति को बदल दिया। भारतीय उप–महाद्वीप के आसपास के क्षेत्र अब समृद्धि का पुल नहीं रहे बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के गैर–औद्योगिकीकरण और विनाश का मार्ग बन गए एवं अधिकांश द्वीप देशों को शाही व्यापार का गुलाम बना लिया। उदाहरण के लिए, मॉरिशस, जिसे यूरोपीय व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्लांटेशन इकॉनमी (बागान अर्थव्यवस्था) बनने को विवश किया गया। फिर से परंपरा चल पड़ी। चूंकि यूरोपीय विजय क्षेत्र समुद्र के माध्यम से प्राप्त हुआ था, ज्यादातर बातचीत, इसकी समुद्री आर्थिक क्षमता की सापेक्ष उपेक्षा के साथ, सुरक्षा और बचाव पर विशेष रूप से जोर देते हुए समुद्र पर केंद्रित थी। [9]
यह याद रखना उपयोगी होगा कि इतिहास के इस पूरे चरण के दौरान जब हिन्द महासागर में भारत की उपस्थिति और विशिष्टता थी। इसे हमेशा द्वीप देशों द्वारा समुद्र में अवसर के रूप में देखा जाता था और कभी भी खतरा नहीं समझा गया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत का कभी भी हिन्द महासागर में आधिपत्य नहीं रहा। दरअसल, आज यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिन्द महासागर के द्वीपों पर कुछ पश्चिमी शक्तियों का झंडा क्यों फहराता रहता है। यह पूछना भी उतना ही प्रासंगिक है कि चीन जैसे क्षेत्र के बाहर के देश यहां नौसैनिक अड्डे क्यों बनाना चाहते हैं। हिन्द महासागर क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षित माहौल को किस प्रकार ये शक्तियां परिवर्तित करना चाहती हैं? क्या हमें, समुद्रतटीय एवं द्वीप राष्ट्रों को चिंतित नहीं होना चाहिए?
हालांकि आज भारत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ सहकारी ढांचे में काम कर रहा है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उनके द्वीप क्षेत्र, सभी औपनिवेशिक अधिकृत प्रदेश, पाश्चात्य देशों के साथ अधीनस्थ संबंधों में क्यों है। इसी तरह, हिन्द महासागर के तटवर्ती और द्वीपीय राष्ट्रों को बाहरी शक्तियों की सुरक्षा शुमार में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? वास्तव में, इससे भी ज्यादा यह बात अस्पष्ट है कि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के पीछे की वजह क्या है। क्या हिन्द महासागर की सुरक्षा एक बार फिर 'बाहरी शक्तियों' के सामरिक हितों दास बन गई है? क्षेत्र के राष्ट्र होने के नाते, हम, इस बारे में क्या कर रहे हैं? इस प्रकार के प्रश्न उत्तर– औपनिवेशिक समाजों के लिए महत्वहीन हैं लेकिन इन सवालों को पूछे जाने और इनका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।
व्यापार पर नवीकृत फोकस
आज़ादी के बाद भारत थोड़ा अंतर्मुखी हुआ और महासागर एवं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान देना कम कर दिया। वर्ष 1991के बाद भारत सरकार ने हिन्द महासागर में भारत के आर्थिक आयामों पर ध्यान देना शुरु किया। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के उदय के साथ–साथ भारत के अपने आर्थिक विकास में तेज़ी ने पश्चिम एशिया से दक्षिण और पूर्वी एशिया में तेल के परिवहन हेतु संचार के समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। यदि हिन्द महासागर में अधिक मात्रा में तेल का परिवहन आरंभ हो जाए तो वस्तुओं के परिवहन में भी तेज़ी आएगी क्योंकि एशिया से यूरोप और पश्चिम एशियाई निर्यात में वृद्धि होगी। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विकास के साथ हिन्द महासागर ने वाणिज्य के क्षेत्र में अपना महत्व पुनः स्थापित किया। पश्चिमी हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की आर्थिक हिस्सेदारी भी पश्चिम एशिया में भारतीय समुदाय की बढ़ती महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका से बढ़ी है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों से आवक प्रेषण समय के साथ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण घटक बन गया है। दूसरी तरफ, खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और आपातस्थितियों में उनकी त्वरित स्वदेश वापसी ने भारत की हिन्द महासागर रणनीति में एक नया सुरक्षा आयाम जोड़ा है।
यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ था और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हिन्द महासागर रिम पहल आरंभ की गई थी, जिससे हिन्द महासागर के तट पर नया क्षेत्रीय समूह बना। आईओआरआई (IORI) को स्थायी विकास एवं क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ आईओआर एसोसिएशन (IORA) में बदल दिया गया। आईओआरए का उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण और सीमा पार व्यापार एवं निवेश बाधाओं को कम करने पर ध्यान देने के साथ महासागर क्षेत्र में सतत विकास एवं क्रमागत उन्नति को बढ़ावा देना है। हालांकि एक संगठन के रूप में आईओआरए (IORA) , जिसका मुख्यालय मॉरीशस में है, ने बहुत धीमी गति से विकास किया है, इसने कम–से–कम भारत में उन मुद्दों पर केंद्रित नीतिगत अवधान में मदद की है जो जल्द ही भारत की ‘नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनमी)’ नीतियों को परिभाषित करने वाली हैं। आईओआरए ( IORA) ने प्राथमिकता के छह क्षेत्रों की पहचान की है जो महासागर क्षेत्र की ‘ब्लू इकॉनमी’ को परिभाषित करती हैं। ये हैं:
- समुद्री सुरक्षा,
- व्यापार एवं निवेश सुविधा,
- मत्स्य प्रबंधन,
- आपदा जोखिम में कमी,
- अकादमिक एवं वैज्ञानिक सहयोग,
- पर्यटन को बढ़ावा देना एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान।
ये आज भी इस क्षेत्र में हमारे मुख्य सरोकार बने हुए हैं।
ब्लू इकॉनमी और क्षेत्रीय सुरक्षा
तीन प्रमुख महासागरीय समुद्र तटों– प्रशांत, अटलांटिक और हिन्द– हिन्द महासागर क्षेत्र आर्थिक रूप से सबसे कम विकसित है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे समृद्ध देशों के बावजूद, महासागर के आस–पास के अधिकांश देशों को न्यून या मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा गया है। हिन्द महासागर में समुद्र– पार व्यापार अटलांटिक और प्रशांत महासागर क्षेत्र में होने वाले समुद्र–पार व्यापार की तुलना में बहुत कम है, जो बहुत हद तक समझ में आता है। वास्तव में, हिन्द महासागर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं अटलांटिक और प्रशांत महासागर के आस–पास के देशों के साथ व्यापार करती हैं। आईओआर (IOR) में और उसके बाहर एकमात्र प्रमुख कारोबारी वस्तु है तेल। क्षेत्र के अपेक्षाकृत आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए, इस क्षेत्र की सरकारों को अपने आंतरिक आर्थिक विकास और शेष विश्व के साथ लाभकारी आर्थिक संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक विकास पर केंद्रित रहने की इस बुनियादी जरूरत को क्षेत्र की सुरक्षा को भी परिभाषित करना चाहिए।
इस समझ को देखते हुए, महासागर–पार संपर्क के विकास, बंदरगाहों, जहाज–निर्माण और समुद्री क्षमता के विकास, मछली पालन और खनिज अन्वेषण, समुद्र विज्ञान आदि पर ध्यान देना क्षेत्र की ब्लू इकॉनमी का विकास एजेंडा होना चाहिए।[10] ब्लू इकॉनमी देश की ‘तटीय अर्थव्यवस्था’ से कहीं अधिक है। इसमें मछली पालन, नाव और जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत और नष्ट करना, बंदरगाह और शिपिंग, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री निर्माण, गहरे समुद्र में खनन, पर्यटन, समुद्री अक्षय ऊर्जा, बीमा, वित्त और महासागर आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं। इसमें देश की बड़ी आबादी को रोजगार और आजीविका प्रदान करने एवं सतत विकास में योगदान करने की क्षमता है। मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका जैसे द्वीपीय अर्थव्यवस्थाओं में ब्लू इकॉनमी के विकास की प्रासंगिकता एवं महत्व पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए, भारत का ब्लू इकॉनमी के विकास पर पर्याप्त ज़ोर देना समझ में आता है। भारत की सुरक्षा और विकास के लिए हिन्द महासागर के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2018 में सिंगापुर में आईआईएसएस (IISS) शांगरी ला वार्ता में कहा था, “हिन्द महासागर ने भारत के इतिहास को आकार दिया है। अब यह हमारे भविष्य की कुंजी है। महासागर के रास्ते भारत का 90% व्यापार होता है एवं हमारे ऊर्जा स्रोत का इतना ही प्रतिशत इसी मार्ग से हम तक पहुंचता है। यह वैश्विक व्यापार की भी जीवन रेखा है। हिन्द महासागर विविध संस्कृतियों और शांति एवं समृद्धि के विभिन्न स्तर वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। अब इसमें विश्व के प्रमुख देशों के जहाज भी आवागमन करते हैं। इससे स्थिरता एवं प्रतिस्पर्धा, दोनों संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं।”[11]
भारत सरकार ने सुरक्षा और विकास के सूत्र सागर (SAGAR)– क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, में हिन्द महासागर में भारत की सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्र के साझा विकास संबंधी प्राथमिकताओं को एक साथ किया है। वास्तव में, सागर (SAGAR) एक भू–आर्थिक निर्माण है जो समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास एवं हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए आवश्यक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह विकास एवं समृद्धि की आवश्यकता के साथ शक्ति एवं सुरक्षा की अनिवार्यता को संतुलित करता है। नतीजतन, हिन्द महासागर के लिए किसी भी समुद्री रणनीति एवं सिद्धांत को इस क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और विकास संबंधी हितों को संतुलित करना चाहिए। दिसंबर 2004 में सुनामी के लिए क्षेत्रीय प्रक्रिया ने अंततः हिन्द महासागर क्षेत्र में विकास और सुरक्षा दोनों के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता की पुष्टि की।
समुद्री डोमेन जागरूकता
ये सभी मुद्दे अब समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए/MDA) कहलाने वाली नीति विचार में एक साथ आ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ/IMO) ने एमडीए को इस प्रकार परिभाषित किया है– “समुद्री पर्यावरण से जुड़ी किसी भी गतिविधि की प्रभावी समझ जो सुरक्षा, सुरक्षा साधन, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है।" समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार हेतु भूमि– आधारित, समुद्र– आधारित, अंतरिक्ष –आधारित और साइबर– संबंधित तकनीकों के उपयोग ने कार्य को अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन एवं आर्थिक रूप से महंगा बना दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने एमडीए में बहुत निवेश किया है और भारत इस क्षेत्र में इन देशों के साथ सहयोग कर रहा है। बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी की लागत और आवश्यक मानवीय क्षमता को देखते हुए छोटे द्वीप राष्ट्र बेहतर एमडीए में निवेश करने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं। एमडीए की बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों का विकास भारत और आईओ (IO) द्वीप राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है।
एमडीए में निवेश को आर्थिक और सुरक्षा, दोनों की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अपनी ब्लू इकॉनमी की क्षमता का दोहन करने के लिए द्वीप राष्ट्रों की क्षमता उनके एमडीए पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, ऐसे राष्ट्रों की सुरक्षा खतरों, विशेष रूप से समुद्र के रास्ते होने वाले आतंकवादी हमले, से बचाव करने की क्षमता भी एमडीए क्षमता पर निर्भर करती है। हिन्द– प्रशांत क्षेत्र में एमडीए क्षमता में सुधार करने के लिए भारत– जापान और भारत – फ्रांस सहयोग हिन्द महासागर के द्वीप राष्ट्रों को लाभान्वित कर सकता है यदि साझा कार्यक्रमों को प्रौद्योगिकी अनुकूलन, सूचना साझाकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ तैयार किया जाए। हिन्द महासागर के द्वीपीय राष्ट्र भारत और समुद्रतटीय एवं द्वीपीय राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के साथ– साथ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में सहयोग की आवश्यकता, दोनों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।
हिन्द महासागर क्षेत्र में भू–राजनीति और भू–अर्थशास्र क्षेत्रीय विकास एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के ढांचे के भीतर काम करने के लिए तटीय और द्वीप राष्ट्रों को विवश करते हैं, इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हिन्द महासागर युद्ध का क्षेत्र नहीं रहा जबकि अटलांटिक और प्रशांत ऐसा बना हुआ है। उदाहरण के लिए तुलना करें, माल्विनास में ब्रिटिश कार्रवाई, क्यूबा के प्रति अमेरिका और ताइवान के प्रति चीन का रवैया। भारत ने हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति कभी ऐसा रवैया नहीं अपनाया। इसकी बजाए, इसने क्षेत्र में विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने की मांग की। यह भारत के हित में है कि वह हिन्द महासागर क्षेत्र के द्वीप राष्ट्रों के साथ पारस्परिक लाभ और पारस्परिक अंतर–निर्भरता के संबंध बनाए रखे, बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता को क्षेत्र को अस्थिर करने की अनुमति न दे।
*****
*संजय बारू,विशिष्ट फेलो,यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।
डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने ।
[1] K.M. Pannikar, India and the Indian Ocean: An Essay on the Influence of Sea Power on Indian History, George Allen & Unwin, London, 1945, 2nd Edition, 1951, p. 23. I found a copy of the 1951 edition in the library of the National University of Singapore. The book bore the stamp “University of Malaya Library. September 1960”. I read this book during my stint at the Lee Kuan Yew School of Public Policy in 2008-09. The book is out of print. I have urged the National Maritime Foundation in India to reprint this classic. Other important studies of Indian maritime activity in the Indian Ocean region include: Ashin Das Gupta, The World of the Indian Ocean Merchant, 1500-1800, New Delhi: Oxford University Press, 2001; and Holden Furber, Sinnapah Arasaratnam and Kenneth McPherson, Maritime India, Oxford University Press, New Delhi, 2004. On the idea of the ‘underlying unity’ of the Indian Ocean region, see K.N. Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge University Press, UK. 1985. For a more recent and popular history of India’s maritime presence in the Indian Ocean region see Sanjeev Sanyal, The Ocean of Churn: How the Indian Ocean Shaped Human History, Penguin Random House, New Delhi, 2016. [2]Hamant Maini and Lipi Budhraja, Ocean Based Blue Economy: An Insight into the SAGAR as the Last Growth Frontier, NITI Aayog, Government of India, at:https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Indian%20Ocean%20Region_v6(1).pdf (Accessed on August 21, 2019);Aparna Roy, Blue Economy in the Indian Ocean: Governance Perspectives for Sustainable Development in the Region, Occasional Paper, January 2019, Observer Research Foundation,. at https://www.orfonline.org/research/blue-economy-in-the-indian-ocean-governance-perspectives-for-sustainable-development-in-the-region-47449/ (Accessed on August 21, 2019).
[3] K.M. Pannikar, no. 1, Chapter 1; Alfred Mahan, The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, Little, Brown and Company, Boston. 1890
[4] Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: Volume II. The Wheels of Commerce, Fontana Press, London , 1982
[5] Ibid., pp. 484-535.
[6] Ibid., pp. 484.
[7] Sanjay Subrahmanyam, ”Introduction”, in Uma Das Gupta (Ed.), Collected Essays of Ashin Das Gupta, Oxford University Press, Delhi. 2001, p. 9.
[8] Ashin Dasgupta, “The Maritime Merchant and Indian History”, in Uma Dasgupta, Ibid., pp. 25-26.
[9]See for example, David Scott, “India’s ‘Grand Strategy’ for the Indian Ocean: Mahanian Visions”, Asia Pacific Review, November 2006; Rahul Roy Chaudhury, Sea Power and India’s Security, Brassey’s, UK, 1999; Rahul Roy Chaudhury, India’s Maritime Security, IDSA, New Delhi, 2000; C. Raja Mohan, Samudra Manthan, Sino-Indian Rivalry in the Indo-Pacific, Oxford University Press, 2013; C. Raja Mohan, Modi and the Indian Ocean: Restoring India’s Sphere of Influence, ISAS Insights No. 277, March 2015; C. Raja Mohan, “India’s New Role in the Indian Ocean”, Seminar, New Delhi, January 2011 at http://india-seminar.com/cd8899/cd_frame8899.html (Accessed on August 21, 2019); Zorawar Daulat Singh, “Foreign Policy and Sea Power: India’s Maritime Role Flux”, Journal of Defence Studies, 11(4), October-December 2017, pp. 21-49.
[10]S. K Mohanty, Priyadarshi Dash, Aastha Gupta, and Pankhuri Gaur, "Prospects of Blue Economy in the Indian Ocean", Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, 2015. at http://www.ris.org.in/sites/default/files/Blue%20Economy_PB_Report_0.pdf (Accessed on August 24, 2019);
Also see Aparna Roy, no. 2.
[11] Narendra Modi, Inaugural Keynote Address to IISS Shangri La Dialogue, Singapore, June 1, 2018. at
https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018 (Accessed on August 24, 2019).