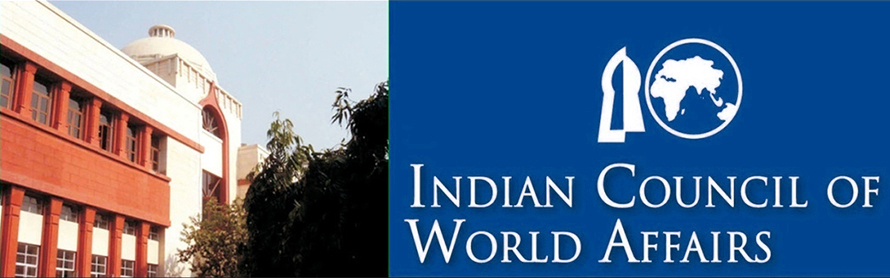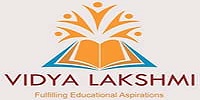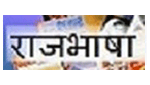भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्लीबदलते विश्व में संवर्धित बहुपक्षवाद को आगे बढाने पर मीडिया विज्ञप्ति, 10 दिसंबर, 2020
विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने 'बदलती दुनिया में संवर्धित बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाना' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया। सम्मेलन में भारत और विदेश के कुल 18 वक्ता शामिल हुएथे। इन वक्ताओं मेंबहु-विषयक क्षेत्रों से संबंधित थे जैसे शिक्षाविद, नीति-निर्माता, राजनयिक और विषय-विशेषज्ञ। वेबिनार के पांच सत्रों और एक पैनल चर्चा में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- भारत और संयुक्त राष्ट्र
- भारत और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय/व्यापारिक संस्थाएं और व्यवस्थाएं
- भारत और अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताएं
- बहुपक्षवाद को पुनःपरिकल्पित करना : भारत का दृष्टिकोण
- भारत के यूएनएससी कार्यकाल 2021-2022 के लिए कार्यसूची
2. वेबिनार की शुरुआत महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूएडॉ. टीसीएराघवन की स्वागत टिप्पणी से हुई। महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूएने कहा कि दो ऐसे संगठनों अर्थात संयुक्त राष्ट्र और लीग ऑफ़ नेशंस, जिनका भारत एक मूल सदस्य था, की क्रमशः 75 वीं वर्षगांठ और शताब्दी, न केवल बहुपक्षवाद के साथ भारत के जुड़ाव पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अवलोकन का उपयुक्त अवसर प्रदान करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय संस्थानों को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक कमजोरी पर एक कड़ी और उचित दृष्टि दौड़ाने का मौका भी प्रदान करती है।उन्होंने सुधार के माध्यम से वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली को संरक्षित करने और मजबूत करने के लिए वैश्विक निकाय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आभासी तौर पर आयोजित वैश्विक शिखर-सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी द्वारा स्थापित किए गए मज़बूत आधार की ओर ध्यान आकर्षित किया…'बहुपक्षवादको समकालीन दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है, केवल एक संवर्धित बहुपक्षवाद, जिसके केंद्र में सुधारा गया संयुक्त राष्ट्र सुधार विद्यमान हो, हीमानवता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए ने रेखांकित किया कि अगले वर्ष जब भारत एक निर्वाचित गैर-स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में आठवीं बार शामिल हो रहा है, 'संवर्धित बहुपक्षवाद प्रणाली के लिए एक नया अभिविन्यास' व्यापक मिशन का गठन करेगा।
3. वेबिनार के पहले सत्र का शीर्षक था 'भारत और संयुक्त राष्ट्र'तथा इसकी अध्यक्षता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अशोक मुखर्जी ने की थी। । इस सत्र में तीन वक्ता शामिल थे- राजदूत मानजीव सिंह पुरी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप-स्थायी प्रतिनिधि, डॉ. अनिरुद्ध राजपूत, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य (2017-2021) और सदस्य, आईसीडब्ल्यूए, शासी परिषद्, प्रो. तस्नीम मीनई, नेल्सन मंडेला शांति और विवाद समाधान केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया।इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र में भारत की गतिविधि और योगदान के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। प्रस्तुतियों मेंअनेक प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने में भारत का योगदान, विशेष रूप से राज्यों के बीच उपनिवेशीकरण और मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के केंद्र में विकास को शामिल करने पर प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्रिस्टलीकरण। यह नोट किया गया कि सैन्य टुकड़ियों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए भारत का योगदान एक विश्वसनीय रिकॉर्ड है और यह यूएनएससीमें स्थायी सदस्यता के लिए भारत के मामले को मजबूत करता है।
4. 'भारत और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय/व्यापारिक संस्थान और व्यवस्थाएं' विषय पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता विकासशील अध्ययन अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के अध्यक्ष, राजदूत मोहन कुमार नेकी। इस सत्र में चार वक्ता शामिल थे, श्री वी. श्रीनिवास, अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, डॉ.अर्चना नेगी, एसोसिएट प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन और निरस्त्रीकरण केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, डॉ.अमितेंदुपालित, सीनियर फेलो एंड रिसर्च लीड (ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स), इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, डॉ.अलोक शील, आरबीआई चेयर इन मैक्रोइकॉनॉमिक्स, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इस सत्र में भारत और अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यापार/वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें संवैधानिक ब्रेटन वुड्स कांफ्रेंस में भारत की भागीदारी शामिल थी, जिसमें कूटनीति और बहुपक्षवाद के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित किया गया था, यद्यपि जहाँ पश्चिमी प्रतिनिधिमंडलों ने अधिपत्य दर्शाया और परिणामों को प्रभावित किया। इसमें आईएमएफ में भारत की भूमिका और उसके साथ संबंध, डब्ल्यूटीओ के प्रति भारत के दृष्टिकोण, विशेष रूप से आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विभेदित परिणामों के परिणामस्वरूप विकासशील देशों के बीच सहयोग से उत्पन्न जटिलताओं का ऐतिहासिक विहंगावलोकन किया गया था।सत्र में यह भी चर्चा हुई कि किस प्रकार वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर अनौपचारिक परामर्श और निर्णय लेने के लिए जी-20 कैसे महत्वपूर्ण हो गया है तथा इसे राजनीतिक-सुरक्षा एजेंडा में शामिल करने के लिए अर्थनीति से परे जाना होगा।
5. 'भारत और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता’ विषय पर तीसरे सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर टी. जयरामन, वरिष्ठ फेलो, एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन, चेन्नई ने की। सत्र के चार पैनेलविद थे - राजदूत मनजीव सिंह पुरी, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि, डॉ. मनीष श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, ऊर्जा और पर्यावरण विभाग, ऊर्जा और संसाधन संस्थान औरडॉ. तेजल कानिटकर, एसोसिएट प्रोफेसर, ऊर्जा, पर्यावरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रगत अध्ययन संस्थान, बेंगलुरु ।इस सत्र में जलवायु परिवर्तन वार्ताओं तथा भारत के विकास के स्थान, विज्ञान के महत्व, जलवायु न्याय तथा राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों और पीढ़ियों के बीच समानता, 'जलवायु कार्रवाई के संबंध में जमीनी स्तर' के रूप में सह-राष्ट्रीय और गैर-राज्य अभिनेताओं की बढ़ती संस्थागत भागीदारीपूर्ण भूमिका के बीच सहसंबंध के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ’यह नोट किया गया कि अब तक भारत एकमात्र ऐसा जी-20 देश है जो पेरिस समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उचित कार्यवाही कर रहा है।
6. 'बहुपक्षवाद की पुनःपरिकल्पना : भारत का दृष्टिकोण' विषय पर चौथे सत्र ’की अध्यक्षता जी.बी. पंत सामाजिक संस्थान, इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय (2005-10) के पूर्व और संस्थापक कुलपति प्रो. राजेन हर्षे ने की थी जिसके अन्य विशिष्ट वक्ता थे, डॉ. अरविंद गुप्ता, निदेशक, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली, डॉ. संजय बारू, विशिष्ट अध्येता, मनोहर पार्रिकर रक्षा और सामरिक विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली, अध्यक्ष, कार्यक्रम समिति, आईसीडब्ल्यूएऔर प्रो. उम्मू सलमा बावा, यूरोपीय अध्ययन केंद्र, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।इस सत्र में बहुपक्षवाद के लिए भूराजनीतिक चुनौतियों, अमेरिका और चीन के साथ संतुलन और सह-अस्तित्व स्थापित करने के संबंध में भारत के प्रयासों की आवश्यकता और उनके बीच प्रतिद्वंदिता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों,मध्यम शक्तियों के साथ बहुपक्षीय एजेंडा विकसित करने की कठिनाइयों, वसुधैव कुटुम्बकमके बढ़ते हएमहत्व, जो कि एक शांतवादी विचार नहीं है, लेकिन जिसका आशय 'हम बनाम उन्हें' सोच को दूर करने की सोच रखता है जोपश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के केंद्र में स्थित है,शक्ति के स्रोतों का रूपांतरण जिसके तहत सैन्य शक्ति से आर्थिक ताकत, यहां तक कि निर्देशात्मक में रूपांतरण किए जाने के बारे में चर्चा की गई।संवर्धित बहुपक्षवाद के संबंध में कार्रवाई करने के लिए यह नोट किया गया किभारत को अपने रणनीतिक उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि क्या यह संकीर्ण संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित संस्थानों पर विशेष बल प्रदान करते हैं या बहुपक्षवाद के व्यापक आयाम पर। मुद्दा-आधारित गठबंधन एक भावी मार्ग हो सकताहै। "साझेदारी के माध्यम से नेतृत्व" के बारे में भारत का दृष्टिकोण,जो इसके भारत-प्रशांत के दृष्टिकोण में अभिव्यक्त किया गया था, एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
7. अंतिम सत्र 'भारत के यूएनएससीकार्यकाल 2021-2022 के लिए एजेंडा'पर राउंड टेबल चर्चा थी। इसकी अध्यक्षता विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. अरविंद गुप्ता ने की, जिसमें तीन वक्ताओं द्वारा भागीदारी की गई थी, अर्थात प्रो.बिमल पटेल, कुलपति, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात, प्रो. प्रियंकरउपध्याय, यूनेस्को चेयर फॉर पीस एंड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉ.मनप्रीतसेठी, प्रतिष्ठित अध्येता, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, नई दिल्ली। यह नोट किया गया कि भारत एक ऐसे समय में यूएनएससी में शामिल हो गया है जो महान शक्तियों की गहन होती प्रतिद्वंद्विता का समय है जिसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन का 'गहन संकट' उत्पन्न हो रहा है जो बहुपक्षवाद को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है, जबकि वैश्विक निरस्त्रीकरण एजेंडा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और नए साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित खतरे उभरकर सामने आए हैं। एक सदस्य के रूप में भारत का हित भारत के हितों की रक्षा करने और साथ ही बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे को बढ़ावा देने में निहित होगा क्योंकि भारत सदस्यों और अवधारणाओं के बीच सहमति निर्माता की भूमिका निभाता है। जबकि निर्वाचित-10 की भूमिका सीमित हो गई है, भारत अनेक एजेंडा मदों पर अपनी पहल को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा जैसे समुद्री सुरक्षा, शांति-व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा इसे अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन पर कार्य करना जारी रखना चाहिए। शांति, सुरक्षा और विकास के लिए उत्तरदायी और समावेशी समाधान; वैश्विक कॉमन्स की सुरक्षा और व्यवस्था; प्रभावी वैश्विक सार्वजनिक माल का वितरण उन प्रमुख विषयों में शामिल होने चाहिए जिनके अनुरूप भारत को अपनी कार्यवाही करनी चाहिए; 'एक संवर्धित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक नए अभिविन्यास' में अतिव्यापी मिशन को शामिल किया जाना चाहिए।
*****